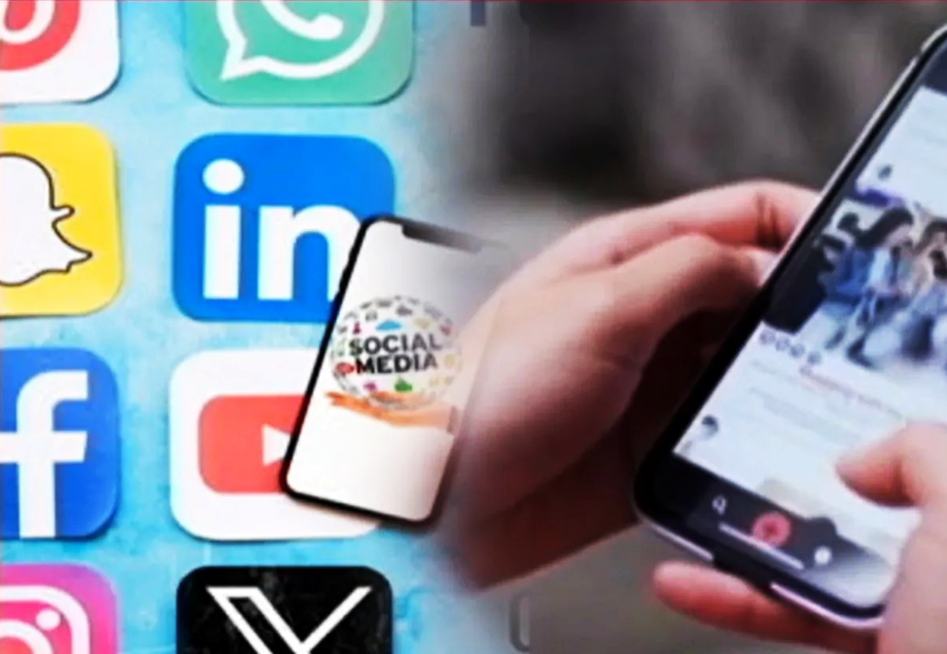डिजिटल उन्माद और सामाजिक विवेक का संकट: सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव
डिजिटल युग ने मनुष्य को अभिव्यक्ति के अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। विचार, सूचना और संवेदना की आवाज अब किसी एक मंच तक सीमित नहीं रही। परंतु जिस माध्यम से लोकतंत्र, पारदर्शिता और सहभागिता सुदृढ़ होनी थी, वही माध्यम आज अनेक बार समाज में भ्रम, विद्वेष और अविवेक का कारण बनता दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने, व्यक्तिगत खुंदक निकालने, ईर्ष्या या राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए तथ्यहीन आरोपों का चलन बढ़ता जा रहा है। ‘न्याय दिलाने’, ‘अभिव्यक्ति की आजादी’, ‘समाजसेवा’ या ‘सरकार और संस्थाओं का विरोध’ जैसे आकर्षक आवरणों में प्रस्तुत की गई सामग्री अक्सर सच से अधिक सनसनी पर आधारित होती है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सोशल मीडिया पर ख्याति, लाइक और फॉलोअर्स की होड़ में व्यक्ति ”कुछ भी कह देने“ और ”कुछ भी कर देने“ को तत्पर दिखता है। एक अधूरी सूचना, एक कटा-छंटा वीडियो या संदर्भ से अलग किया गया कथन। बस इतना ही पर्याप्त होता है किसी व्यक्ति, संस्था या प्रक्रिया के विरुद्ध जनाक्रोश खड़ा करने के लिए। परिणामस्वरूप, जब विधिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत कार्यपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका से जुड़ी कोई आवश्यक कार्रवाई की जाती है, तो बिना तथ्य समझे, बिना मामले की जटिलताओं को जाने, तीखी प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। विवेक के स्थान पर आवेग और प्रमाण के स्थान पर पूर्वाग्रह हावी हो जाता है।
यह आवेगात्मक प्रतिक्रिया-तंत्र समाज में एकतरफा नरेटिव गढ़ता है। सत्य बहुआयामी होता है उसमें समय, साक्ष्य, संदर्भ और विधि की भूमिका होती है। किंतु सोशल मीडिया का एल्गोरिदमिक ढांचा अक्सर उसी सामग्री को आगे बढ़ाता है जो भावनाओं को भड़काए। इस प्रक्रिया में संतुलित दृष्टि, धैर्य और सुनवाई का अवसर सिकुड़ता चला जाता है। परिणामस्वरूप नकारात्मकता फैलती है, संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता है और सामाजिक ताने-बाने में दरारें पड़ती हैं।
अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का प्राण है, पर वह निरंकुशता का लाइसेंस नहीं। स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। जब तथ्य जांच (फैक्ट-चेकिंग) को दरकिनार कर अफवाहें साझा की जाती हैं, जब निजी जीवन को सार्वजनिक तमाशा बनाया जाता है, या जब न्यायिक प्रक्रियाओं को ‘ट्रायल बाय सोशल मीडिया’ में बदल दिया जाता है, तब यह स्वतंत्रता स्वयं अपने उद्देश्य से भटक जाती है। ऐसी प्रवृत्तियां न केवल व्यक्ति विशेष को क्षति पहुंचाती हैं, बल्कि समाज के सामूहिक विवेक को भी कमजोर करती हैं।
एक और दुष्प्रभाव है- ध्रुवीकरण। सोशल मीडिया की तेज रफ्तार प्रतिक्रियाएं विचारों के बीच संवाद नहीं, बल्कि खेमेबंदी को बढ़ावा देती हैं। असहमति का स्थान गाली-गलौज ले लेती है और तर्क की जगह ट्रोलिंग। इस वातावरण में सच की तलाश कठिन हो जाती है और सामाजिक विश्वास का क्षरण होता है। जो संस्थाएं कानून और न्याय की रीढ़ हैं, उन पर अविश्वास पैदा होना अंततः लोकतांत्रिक ढांचे को ही कमजोर करता है।
इस चुनौती का समाधान सेंसरशिप या चुप्पी नहीं, बल्कि शिक्षित और जिम्मेदार सहभागिता है। एक शिक्षित समाज से अपेक्षा है कि वह सूचना को साझा करने से पहले उसके स्रोत, संदर्भ और सत्यता की जांच करे। त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखे; ‘सुना’ और ‘देखा’ के बीच के अंतर को समझे। नागरिक डिजिटल साक्षरता को अपनाएं, एल्गोरिदम की प्रकृति, क्लिक-बेट की रणनीति और भावनात्मक हेरफेर को पहचानें। संस्थाएं पारदर्शिता बढ़ाएं और समय पर तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि अफवाहों के लिए स्थान न बचे।
अंततः, सोशल मीडिया स्वयं में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग उसे परिभाषित करता है। यदि हम इसे न्याय, करुणा और विवेक के साथ प्रयोग करें, तो यह समाज को जोड़ सकता है; यदि आवेग, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के साथ, तो यह हमें अंधे मोड़ की ओर ले जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम डिजिटल नागरिकता के मूल्यों को अपनाएं, सत्य के प्रति निष्ठा, असहमति में शालीनता और अभिव्यक्ति में उत्तरदायित्व। तभी हम नकारात्मकता के इस जाल को कम कर पाएंगे और एक स्वस्थ, संतुलित तथा न्यायप्रिय समाज की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।
लेखक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में प्रोफेसर है।