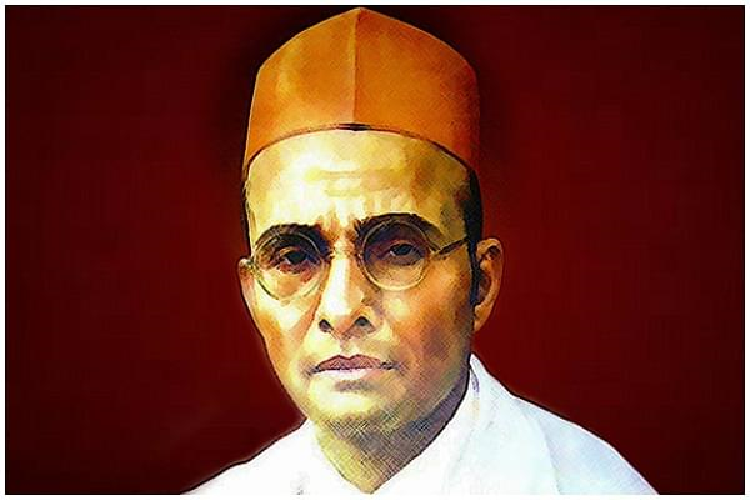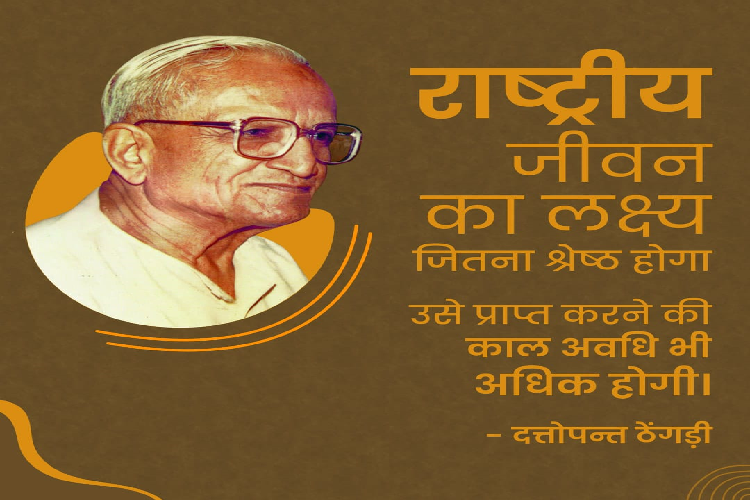समाज के पंच परिवर्तन
लेखक - राम कुमार शर्मा
देश के वातावरण और वैश्विक परिदृश्य में भारत के प्रति सोच बदली है। देश एक बड़े परिवर्तन की बाट जोह रहा है। अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ भी सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ पुण्यभूमि भारत के उत्कर्ष के लिए संकल्पबद्ध होकर जुट गया है। संघ समाज का संगठन है इसलिए समाज का प्रत्येक सदस्य नये भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हो, राष्ट्र के परम वैभव हेतु समाज के एक-एक सदस्य का योगदान हो, इसी दृष्टि से संघ ने सम्पूर्ण भारतीय समाज में आधारभूत परिवर्तन के लिए जिन पांच आयामों को चुना है वे हैं - ‘स्व’, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण और नागरिक कर्तव्य।
सामाजिक समरसता: राष्ट्र और समाज में विविधता होना सहज एवं स्वाभाविक है। विविधता में एकता के लिए एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे खान-पान रहन सहन, भाषा, वेशभूषा अलग हो सकते हैं परन्तु जब राष्ट्र की बात आती है तो हम विविधता होते हुए भी एक साथ कार्य करें। एकता के लिए मन का भाव मिलना जरूरी है। समता लक्ष्य है, समता आधार है। व जन्म, वृत्ति रंग के आधार पर ऊँच-नीच, अगड़ा पिछडा यह भेद हमारे राम और कृष्ण ने भी कभी जाति के आधार पर भेद नहीं किया तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे साधु सन्तों ने भी और गुरुओं ने भी शिक्षा और संस्कार प्रक्रिया में भेद नहीं माना तब हम लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं! समाज में सामाजिक समरसता की भावना जगी, मन्दिरों, गांव, कुआँ, वेदों का पठन पाठन, स्पर्शबंदी आदि बहुत सी कुप्रथा पनपाने का कार्य विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा रख समाज को कमजोर करने वाले विचार पनपाये गये जिससे सामाजिक समरसता का भाव नहीं पनप सका। मन और हृदय से समरसता आती है। समस्त हिन्दू समाज देश है यह मानना, उसकी प्रगति मेरी भी प्रगति है। यह जानकर व्यवहार करना। ऊँच-नीच हुआ-छूत छोटा-बड़ा, अमीर गरीब का भाव त्यागकर हमारे स्वयं के आचरण से ही होगा।
कुटुम्ब प्रबोधन: वर्तमान समय में कुटुम्ब प्रबोधन व्यवस्था का हास होता दिखाई दे रहा है। संयुक्त परिवार कुटुम्ब परिवार, संस्कार, धर्म, संस्कृति हमारी पहचान रही है। परन्तु आज हमारी पीढ़ियाँ इन सबसे दूर होती दिखाई दे रही हैं। अतः अब इस और प्रयास करने की आवश्यकता है। परिवार की दिनचर्या का विकास करना जिसमें अपने घर में परिवार के साथ सत्संग करना। कुटुम्ब, मित्र बनाना। भोजन, भजन, भ्रमण, संवाद, भाषा, भूसा में परिवर्तन करना। इन सब बातों की शुरुआत हमें स्वयं के परिवार से शुरू करनी होगी। परिवार के लोगों का एक साथ बैठकर भोजन, भजन, भ्रमण, वेशभूषा, बातचीत के द्वारा प्रयास करके वातावरण बनाना। अपने परिवार में संयुक्त का वातावरण बनाकर हम अपने परिचित स्वयंसेवकों, परिचितों को प्रेरित कर परिवर्तन ला सकते हैं। अपने स्वयं के तथा परिचितों के परिवारों में परिवर्तन कर हम उनके आस-पास निवास कर रहे परिवारों में भी कुटुम्ब प्रबोधन का सतत प्रयास करें। हमें अपने परिवारों, परिचितों तथा परिचितों के आसपास वाले परिवारों के साथ मिलकर होली, दीपावली सुन्दर कांड, स्वदेशी वस्त्र पहिनना आदि कार्यक्रम सामूहिक रूप से मनाने पर संस्कृति और संस्कार बचेंगे।
पर्यावरणः पर्यावरण के संदर्भ में गत दो दशकों से राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन चल रहा है। देश भर में हम प्रकृति असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। इन सब परिवर्तनों का सम्बन्ध मनुष्य से ही जुड़ा हुआ हैं। आँधी, तूफान, बाद, भूस्खलन आदि प्रकृति का दोहन होने के कारण यह समस्यायें होती जा रही हैं। मनुष्य के द्वारा, पेडों का कटान, खनन भवन निर्माण आदि के माध्यम प्रवृत्ति के साथ जीवन का सन्तुलन बिगड़ रहा है। हमारी जीवन शैली में यदि परिवर्तन नहीं आया तो इसका समाधान होना असम्भव सा लगता है।
गन्ध युक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु सभी मेरे प्रातरू को मंगलमय करें यह तभी संभव होगा जब हम प्रकृति का शोषण. दोहन सीमित और संतुलित मात्रा के अनुरूप करेंगे।
जल, जमीन, जंगल, प्लास्टिक के उपयोग में सचेत होने पर ही हम पर्यावरण का संरक्षण करने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।
जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है।
अन्यथा इसके अभाव में वैश्विक युद्ध जल को लेकर हो सकता है। अतः एक एक बूँद पानी का संरक्षण आवश्यक है।
वृक्षारोण का महत्व पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने हेतु अत्यावश्यक है। अतः अधिकाधिक लोगों को पीपल, बरगद नीम, इमली बेल आदि लगाने से पर्यावरण संरक्षित होगा! अपने आस पड़ोस का वातावरण स्वच्छता शुद्ध बनाये रखने हेतु लोगों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है। नदियों का जलस्वच्छ बनाये रखने हेतु नदियों को स्वच्छ रखने के प्रयास हों। घर परिवारों को हरित बनाने का प्रयास सार्वजनिक स्थल, शाखा स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु हम क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं पर चर्चा वार्ता कर प्रेरित करना।
स्वदेशी: स्वदेशी भाव का जागरण एक पुनीत कार्य है यह केवल अर्थ से जुड़ा विषय नहीं है! माता पिता मित्र. भाई रिश्तेदार, (पृथ्वी आकाश वायु, जल, अग्नि ये पंच महाभूतों को मेरा प्रणाम है। मेरा अपना देश आत्म निर्भर, स्वावलम्बी बने इस हेतु हमें कुटीर, ग्रामीण कृषि आदि कार्यों को बढ़ावा देने से ही हम स्वदेशी का भाव लोगों के अन्दर भर सकते हैं।
घर, विद्यालय, परिवार और समाज में स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह करें चर्चा करें, देश मे निर्मित सामग्री हम अपने जीवन में प्रयोग कर स्वदेशी का भाव जन-जन तक पहुँचायें और अपनायें विदेशी सामग्री का त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं का भरपूर उपयोग करें ऐसे भाव लोगों को समझाने का प्रयास हो। आज अधिकांश लोग विदेशी सामग्री खान-पान की वस्तुएँ वस्त्र साज-सज्जा सामग्री खेल खिलौने आदि की ओर आकर्षित होते दिखाई देते हैं। इन सब से मोह भंग करने हेतु स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता, आदि चीजों की ओर ध्यान देकर राष्ट्रीय भाव जाग्रत करने की दिशा में हम सभी प्रयास करें।
नागरिक कर्त्तव्य: वर्तमान समय में नागरिक कर्तव्य का पालन ही सच्ची देशभक्ति है। केवल वातों से नहीं अपितु कृति से अपने नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें तभी हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक श्रेष्ठ नागरिक कहलाने के सही अर्थाे में अधिकारी हैं। इसीलिये गीत की निन्न पक्तियों में कहा गया है कि -
जियें देश हित, मरें देश हित
तिल-तिल कर गल जाना सीखें
व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है परन्तु देश, समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों को भूल जाता है।
राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान करना हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा व्यवहार घर, कार्यालय, बस ट्रेन, दुकान आदि पर एक सभ्य समाज के नाते होना चाहिये। हमें समाज को संघटित एवं सुसंस्कारित बनाना है।
आज राष्ट्रीय सम्पत्ति का अधिकांश मात्रा में नुकसान कुसंस्कारों, राष्ट्रीय भावों का अभाव के कारण हो रहा है। न राष्ट्रीय गान, न राष्ट्रीय आदि का सम्मान किया जा रहा है।
मातृभूमि के लिये हमारा व्यवहार कैसा हो ? उसके प्रति संवेदना कैसी हो पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
देश की रक्षा करें और आहवान किये जाने पर राष्ट्रीय सेवाए प्रदान करें !
प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें, और अधिकारों पर बल न देकर देश की संप्रभुता और अखण्डता की रक्षा कर अपना कर्तव्य निभायें।