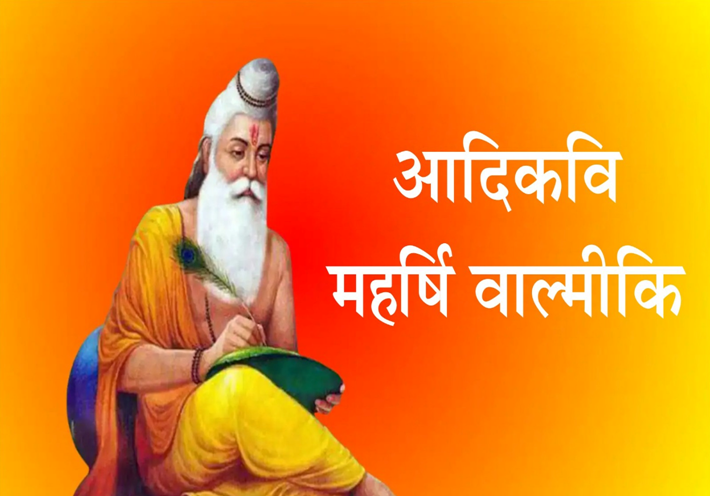विश्व की पहली कविता का पहला पुरस्कार!
महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है, क्योंकि उनसे पहले विश्व ने केवल वैदिक मंत्र सुने थे, जिन्हें अपौरुषेय कहा गया है। विद्वानों के समाज में आदिकवि के महाकाव्य को ‘आर्ष रामायण’ मानते हुए उसे सार्वकालिक काव्यबीज कहा गया-काव्यबीजं सनातनम्। यानी विश्व की सारी कविताओं का उत्स यही है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम का मार्ग (अयन), जिसके जीवनादर्शों पर अनंत काल तक मानव सभ्यता चल सके और जिसके निकष पर किसी देशकाल की सभ्यता- संस्कृति को आँका जा सके। महाभारत, भागवत और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास ने ‘स्कंद पुराण’ में महर्षि वाल्मीकि की जीवनी बहुत श्रद्धापूर्वक लिखी है। पुराणों में यह भी चर्चा है कि यदुवंशी लोग रामायण पर आधारित नाटक खेलते थे- रामायणं महाकाव्यमुद्दिश्य नाटकं कृतम्। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ‘रामचरित मानस’ को लोकजीवन में उतारने के लिए काशी में रामलीला का सूत्रपात किया।
वैसे तो लोकजीवन में देवर्षि नारद को हास्य का पात्र बना दिया गया है, जिसका असर पौराणिक फिल्मों पर भी पड़ा है, लेकिन वाल्मीकीय रामायण का शुभारंभ नारद के गुणगान से होता है और उसका पहला शब्द ‘तप’ है-
तपःस्वाध्याय-निरतं तपस्वी वाग्विदांवरम्।
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्।।
महर्षि वाल्मीकि तप और स्वाध्याय में निरत, कुशल वक्ता, मुनिपुंगव नारद से पूछते हैं कि इस समय संसार में सबसे बड़े गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रती कौन हैं? इस पर, तीनों लोकों के ज्ञाता नारद जी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न दाशरथि राम के गुणों का वर्णन करते हुए राम का चरित वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ राजा दशरथ अपने प्रजा-वत्सल ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं और उस तैयारी को देखकर रानी कैकेयी पूर्व में दिये गये वरों का संदर्भ देते हुए राजा दशरथ से राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक माँगती हैं-विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। राम का चरित्र यहीं से उभरता है, जब वे युवराज की पात्रता रखते हुए भी कैकेयी का प्रिय करने के लिए, पिता के निर्देश का पालन करते हुए वन चले जाते हैं। उसके बाद होने वाली सारी रामकथा संक्षेप में त्रिकालदर्शी नारद महर्षि वाल्मीकि को सुनाते हैं। अंत में वे रामराज्य का वर्णन करते हुए भविष्य की रूपरेखा भी खींचते हैं कि 11 हजार वर्षों तक राज्य करने के बाद श्रीराम ब्रह्मलोक चले जाएंगे (ब्रह्मलोकं प्रयास्यति)।
अभी तक वाल्मीकि केवल तपस्वी थे। देवर्षि के मुंह से सीता और राम की अलौकिक कथा सुनकर उनके भीतर करुणा की धारा बह निकली। महामुनि नारद के प्रस्थान करने के बाद वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज से वल्कल लेकर तमसा नदी के तट की ओर स्नान करने गये। वे विशाल वन में विचर ही रहे थे कि एक मर्मान्तक घटना घटी। वहाँ क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा प्रेमक्रीड़ा कर रहा था कि एक निष्ठुर व्याध ने वाण चलाकर नर क्रौंच को मार डाला। रक्त से लथपथ उस पक्षी के भूमि पर गिरते ही क्रौंची चीत्कार कर उठी। इस कारुणिक दृश्य से विकल होकर धर्मात्मा वाल्मीकि के मुँह से निषाद को संबोधित यह अनुष्टुप श्लोक निकल पड़ा-
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।
(निषाद, तुझे कभी स्थायी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस निरपराध क्रौंच जोड़े में से एक काममोहित को मार डाला।)
कहने को तो महर्षि कह गये, मगर बाद में उन्हें लगा कि यह तो चार चरणों में आबद्ध, बराबर अक्षरों वाला श्लोक है, जिसे वीणा पर गाया जा सकता है। स्नान कर मुनि शिष्य भरद्वाज के साथ आश्रम लौटे, संध्या वंदन के लिए आसन पर बैठ भी गये, मगर उनके मन में वह श्लोक अटका रहा। तभी अखिल सृष्टि की रचना करने वाले, चतुर्मुख ब्रह्मा महर्षि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम आये। परम विस्मित होकर महर्षि ने ब्रह्मा जी का स्वागत-सत्कार किया। जब दोनों उपयुक्त आसन पर बैठ गये, तब महर्षि ने क्रौंच-वध और उसके बाद उनके मुख से शाप रूप में निकले श्लोक की चर्चा की। तब ब्रह्मा जी ने हँसकर कहा कि मेरी प्रेरणा से ही आपकी जिह्वा पर सरस्वती श्लोक रूप में अवतरित हुई है। अभी नारद जी ने जो धीर और धर्मात्मा श्रीराम के जीवन का वर्णन आपसे किया है, उसे काव्य में अभिव्यक्त करिये। ब्रह्मा जी ने श्रीराम, सीता, लक्षण और राक्षसों के सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट वृत्तांत को जानने की दिव्य शक्ति उन्हें दी और कहा कि इस काव्य में कोई भी बात झूठी नहीं होगी-न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। ब्रह्माजी ने वरदान दिया कि पृथ्वी पर जब तक नदी-पर्वत रहेंगे, तबतक रामायण की कथा लोक-जीवन में प्रवाहित रहेगी-
यावत्स्थास्यंति गिरयः सरितश्च महीतले।
तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।।
साथ ही, जबतक राम की कथा रहेगी, तब तक आपकी प्रतिष्ठा तीनों लोकों में रहेगी। यह कहकर ब्रह्मा जी समस्त आश्रमवासियों को विस्मय में डालकर अंतर्धान हो गये।
ब्रह्मचारी गण उसी एक श्लोक को बारंबार वीणा पर गाने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही श्लोकों में पूरा रामायण रचने का संकल्प किया। उस समय तक लिपि का विधिवत विकास नहीं हुआ था, इसलिए सारा काव्य-संभार वेदों की भाँति वाचिक यानी मौखिक ही था। इसलिए महर्षि ने कुशासन पर बैठकर, समाधि लगाकर पूरे वृत्तांत का साक्षात्कार किया। उन्होंने राम-लक्ष्मण-सीता, रानियों सहित राजा दशरथ के हँसने-बोलने आदि सभी चेष्टाओं और सम्पूर्ण राष्ट्र की गतिविधियों का अपने योगधर्म से यथावत साक्षात्कार किया। यहाँ तक कि योग बल से उन्होंने भूत-वर्तमान-भविष्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने राम के जन्म से लेकर वनवास, सेतुबंध, रावण आदि राक्षसों का वध, राम का अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक, राजधर्म के कारण वैदेही का वन में त्याग, लव-कुश का जन्म आदि समस्त घटनाओं का विस्तृत वर्णन रामायण में किया। महर्षि ने छह काण्डों, 5 सौ सर्गों और 24 हजार श्लोकों में पूरे रामायण की रचना की-
चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः।
तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्।।
‘रामायण’ या ‘पौलस्त्य वध’ महाकाव्य तो रच गया। अब महर्षि को चिंता हुई कि इतने विशाल महाकाव्य को आत्मसात् कर कौन व्यक्ति जन समुदाय को सुनाएगा? तभी आश्रम में रहने वाले वटु-द्वय कुश और लव महर्षि के पास आए। अत्यंत सुरूपवान दोनो भाई राम के प्रतिरूप लगते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी, मधुर स्वर भी था और दोनों वेदों में पारंगत हो चुके थे। महर्षि दोनांे भाइयों को सुयोग्य मानकर वीणा पर स्वर-ताल से रामायण का गायन सिखाने लगे। यथा समय दोनांे भाइयों ने सम्पूर्ण महाकाव्य को कण्ठस्थ कर लिया और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता था, तब उनके बीच बैठकर दोनों भाई एकाग्रचित्त होकर रामायण का गान करने लगे।
एक बार ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण वाले वनवासी ऋषि-मुनियों की सभा हुई, जिसमें महात्माओं के बीच बैठकर जब कुश-लव ने रामायण के श्लोकों को गाना शुरू किया, तो उसे सुनकर महात्माओं की आँखें भर आयीं। सभी साधु-साधु (वाह-वाह) कर उठे और कुमारों के मधुर गायन और श्लोकों के माधुर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे-अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानाञ्च विशेषतः। वे सोचने लगे कि यद्यपि यह घटना बहुत पहले ही हो चुकी है (चिरनिर्वृत्तमप्येतत्), तथापि प्रस्तुति इतनी सजीव थी कि लगा, पूरी घटना आँखों के सामने हो रही हो। प्रसन्न होकर किसी मुनि ने दोनों कुमारों को कलश प्रदान किया, किसी ने वल्कल। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया, किसी ने जनेऊ (यज्ञसूत्र)। एक ऋषि ने कमण्डलु दिया तो दूसरे ने मूँज की मेखला। तीसरे ने आसन तो चौथे ने कौपीन (लँगोटी) प्रदान किया। एक मुनि ने हर्षित होकर कुठार दिया। किसी ने काषाय (गेरुआ वस्त्र) तो किसी ने चीर (वस्त्रखंड) दिया। किसी मुनि ने खुश होकर जटा बाँधने की रस्सी (जटाबन्धन), किसी ने समिधा बाँधनेवाली डोरी (काष्ठरज्जु), किसी ने यज्ञभाण्ड (यज्ञ का बरतन), किसी ने काष्ठभार( तिनके से निर्मित जूना) तो किसी ने गूलर की लकड़ी से बना पीढ़ा अर्पित किया। किसी ने दोनों कुमारों के दीर्घायु होने का आशीष दिया और किसी ने दोनों के कल्याण की कामना की। सभी सत्यवादी मुनियों ने दोनांे कुमारों को नाना प्रकार के वरदान दिये और महर्षि वाल्मीकि के अद्भुत काव्य को सराहते हुए उसे परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधार माना।
इस प्रकार, विश्व की पहली बड़ी कविता के रचयिता को मनीषियों की मुक्तकंठ प्रशंसा मिली और उसका गान करने वाले दोनों कुमारों को जीवन का पहला सात्विक पुरस्कार।