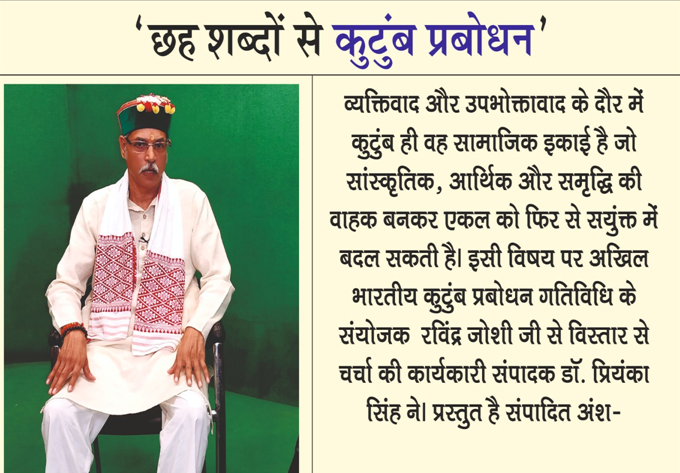‘छह शब्दों से कुटुंब प्रबोधन’
भारतीय संस्कृति में क्या कुटुंब और परिवार अलग हैं ?
थोड़ा शब्दों में बोल सकते हैं। हमारे पूर्वजों की दृष्टि इतनी विशाल थी कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग एक ही परिवार के हैं। इस भावना से हमें रहना है। संस्कृति में कुटुंब है और हिन्दी में परिवार चलता है। कुटुंब में अपने रक्त से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनका विचार और परिवार में व्यापक रूप में जैसे हमारे अड़ोस-पड़ोस के हैं, हमारा घर चलाने में जिनका सहयोग मिलता है, वे भी अपने ही परिवार के हैं। ऐसा उनके साथ प्रेम, आदर, विश्वास का व्यवहार करना और केवल मनुष्य नहीं, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी अपने घर में, यदि किसी के घर में गाय है तो वह भी अपने परिवार की ही है। ऐसा व्यवहार हमारे यहां रहा है। हम सबने चंदा मामा वाली बात सुनी है ऐसे सारे विश्व के साथ यह जो नाता जोड़ने की दृष्टि है, भारत की विशेषता है।
संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन में से एक है कुटुंब प्रबोधन, संघ की दृष्टि में यह क्या है?
उसमें एक बात ऐसी है कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको कम से कम सप्ताह में एक बार एकत्रित होना है। भोजन करना है, ईश्वर का स्मरण करना है और उसके बाद एक डेढ़ घंटा अच्छी गपशप करना है। अब सहज रूप से प्रश्न आ सकता है कि गपशप की बातें क्या रहेंगी? तो एक छोटा सा वाक्य हमने बताया है कि जो आठ से पंद्रह दिन में हम कहीं घूमकर आयें हैं। क्या अच्छा देखा, सुना, पढ़ा, सीखा है? इसके अपने सारे अनुभव साझा करना। साथ ही अपने परिवार में माँ की ओर से तीन चार पीढ़ियां, पिताजी की ओर से तीन चार पीढ़ियां उनकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं और वह आपस में बताना है। घर में वातावरण बनाना, भक्ति, शक्ति, आनंद में अपना घर बनाना इसकी बातें करते हैं।
बदलते हुए वैश्विक और वर्तमान परिदृश्य में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता क्यों है?
हम सबको पता है कि आज सारे समाज पर ही नहीं पूरे विश्व पर भोगवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उपभोक्तावाद कहते हैं या थोड़ी उच्छृंखलता है। भारत की विशेषता यानी भारत की जीवनदृष्टि, जीवन मूल्य हैं। उसके आधार पर जीवन व्यवहार है तो उसमें थोड़ा क्षरण आ रहा है। उसके सामने समस्याएं निर्माण हुई हैं बाहर के वातावरण के कारण। इसलिए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हम बात करते हैं कि छह शब्द है भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन और भ्रमण। ये छह बातें हम अपने भारतीय दृष्टिकोण से जीवन व्यवहार में करते हैं। यह करने से कुटुंब में एक अच्छा वातावरण रहता है।
आज जिस तरह से कुटुंब में संवादहीनता खत्म हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
मूल समस्या यही है कि व्यक्तिवाद और करियर के प्रभाव से परिवार बिखर रहे हैं। सहज रूप से परिवार में एक साथ बैठना यही उसका उत्तर है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है कि सभी कामों का अधिष्ठान अपना अध्यात्म है, ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हुए सारी बातें करना तो घर में पहले से वातावरण बनाना, एक साथ बैठना, यह करने के बाद दूसरे के मन में क्या है, यह समझने के लिए थोड़ा सा अपना मन बनाना। आजकल लोग बाहर से आने के बाद घर में भी सब गैजेट्स से जुड़े रहते हैं। उसके स्थान पर जब हम बैठेंगे तो यह मोबाइल और टीवी बाजू में रखना है। एक बहुत अच्छी संकल्पना विकसित हुई है मोबाइल पार्किंग। हमको स्कूटर पार्किंग, कार पार्किंग मालूम है। हमारे गोवा में एक बहन हैं तो उन्होंने कहा कि पहले बड़ी समस्या थी आपस में संवाद नहीं करना, बात नहीं करते थे। तो इसका उत्तर बताया मोबाइल पार्किंग। घर में और सामूहिक रूप से भी जब हम इकट्ठा होते हैं तो अभी यह आदत विकसित हो रही है कि मोबाइल को थोड़ा अलग रख देना और बात करने के लिए बैठना। उसके माध्यम से एक संवाद के लिए अनुकूलता का निर्माण होता है।
पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परागत रूप से विकसित होती आई भारतीय जीवन शैली कुटुंब व्यवस्था की ही देन है इस पर प्रकाश डालिए?
हां, कुटुंब प्रबोधन का विषय ऐसा है कि केवल संघ के स्वयंसेवक ही काम करें, ऐसा नहीं है। अपने भारतवर्ष में सर्वप्रथम यह स्वामीनारायण संप्रदाय के जो प्रमुख स्वामी थे, उन्होंने इस विषय को 1975 में प्रारंभ किया। फिर आज हम देखते हैं कि गायत्री परिवार है, चिन्मय मिशन है, गीता परिवार है और कई संत सत्पुरुष, माता अमृतानंदमयी हैं। परंपराओं को हमारे भारत में सहजता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाना यह बहुत सहजता से होता है। यह सभी लोग इसे कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूं तो वहां का एक उदाहरण लेता हूं। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। चित्रा मिठाई वाले पूना में रहते हैं। उनकी चौथी पीढ़ी से मैं मिला, तो उनकी जो पहली पीढ़ी के व्यक्ति जिन्हांेने यह सारा व्यवसाय विकसित किया, उनका नाम था भास्कर। उनको जब अपनी जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी को देनी थी तब उन्होंने कहा कि जब आपके मन में दूध में पानी मिलाना ऐसा विचार आएगा तो यह चित्रा मिठाई दुकान बंद कर देंगे।
बच्चों के सही मार्गदर्शन और पालन-पोषण में कुटुंब प्रबोधन की क्या भूमिका है?
सारे परिवार, विशेष रूप से दोनों कमाने वाले जहां है, वहां तो यह समस्या बहुत अधिक है। पहली बात समझना बहुत आवश्यक है। आज की पीढ़ी में जो नए बालक आ रहे हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं। इसका भी एक अलग प्रकार से अध्ययन होना चाहिए। लेकिन यह भावना और संस्कार वाली है। इसमें मैं पूना का एक अनुभव आपको बताता हूं। ऐसे ही एक परिवार में सब लोग कमाने वाले थे, बाहर जाने वाले थे। चार वर्ष का छोटा बालक था जिसे सबके मोबाइल के पैटर्न्स मालूम थे। मोबाइल कैसे खोलना, देखना सब आता था जिससे उसके पिताजी और दादाजी बड़े परेशान थे। अब इसका उपाय क्या करना? पहला उपाय उन्होंने यह किया कि सबके पैटर्न बदल डाले, तब उसको खोलने में दिक्कत आने लगी तो चिड़चिड़ापन होने लगा। लेकिन उसी के साथ वह कैरम लेकर आए और भोजन के पहले या बाद में उसके साथ बैठकर कैरम खेलना शुरू कर दिया। अब वह बालक मोबाइल को पूछता भी नहीं है। इसलिए ध्यान में आता है कि हम जो बातें कर रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों के लिए एक अच्छा समय देना, उनके साथ समय बिताना चाहिए। इस क्रम में छोटे-छोटे खेल हो सकते हैं। कहानियां बताना हो सकता है ऐसा करने से वे अपनी संस्कृति और संस्कार ग्रहण करेंगे। बड़ों के प्रति आदर का भाव निर्माण करना है जो हमको करना चाहिए। भारत में संस्कृति की दृष्टि से वह सहजता से आएगा। छोटे-छोटे त्यौहार रहते हैं। उसमें आजकल सारा रेडीमेड लेकर आना है, ऐसा चलता है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से जैसे गणेश जी का त्यौहार हुआ तो चर्चा में ऐसी बातें निकली कि घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाना, गणेश जी की मूर्ति बनाने की थोड़ी सी कला सिखाना, तो उसके कारण एक अलग वातावरण बनता है। गणेश जी की सजावट सबको मिलकर करनी है। इस प्रकार का घर में एक वातावरण बने और यदि एक-एक, दो-दो, अड़ोस-पड़ोस के कई परिवार मिलकर इकट्ठा आएं वह करें तो उसका भी अनुभव हमको बहुत अच्छा आता है।
संगठन के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन के संबंध में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं?
मेरे पास पूरे भारत का अखिल भारतीय संयोजक ऐसा दायित्व है। ऐसे भारतवर्ष में अपने 45 प्रांत हैं। इसमें अधिकतर प्रांतों के संयोजक नियुक्त हैं। उनके माध्यम से आयु अनुसार कुछ उपक्रम अपने-अपने स्थान पर करते रहते हैं। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हमने दो उपक्रमों को सोचा है। एक है 14 अगस्त से 29 अगस्त तक। यानी हमारा देश स्वाधीन हुआ 15 अगस्त को। भारत का इतिहास देखेंगे तो बार-बार इस राष्ट्र पर आक्रमण हुए, राज्य गया, फिर से आया। ऐसे कई बार हुआ है पिछले दो हजार वर्षों में। लेकिन देश का विभाजन नहीं हुआ था। यदि 500 वर्ष बाद राम का मंदिर निर्माण हो सकता है तो इस राष्ट्र के अंदर अखंड भारत के प्रति भी एक जागृति यदि हम कायम रखेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा। हम सबको पता है कि महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1947 का उनका जो रेडियो का भाषण है, उसमें महर्षि अरविंद ने कहा है कि ”आज इस देश का विभाजन हुआ है, लेकिन यह देश अखंड होकर रहेगा। इसकी कई कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको संघर्ष करना होगा, सारी बातें होंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, यह अखंड होगा।“ उस बिंदु को हमने पकड़ा है कि घर-घर में अपने परिवार के अड़ोस-पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करना। यह जो 14 अगस्त से 29 अगस्त का कालखंड है, 29 अगस्त को अपने देश के एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। उनका जीवन भी बहुत प्रेरणादायी है। उनके जीवन की कहानियां, ऐसे ही अपने राष्ट्र को जिन्होंने उन्नत किया, स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लिया। मेरठ से 1857 की क्रांति का शंखनाद ऐसी सारी बातों पर नयी पीढ़ी के साथ बैठकर चर्चा करना। अच्छे छोटे-छोटे खेल खेलना। उसके लिए हमने खेल का एक ऐप भी बनाकर पूरे भारतवर्ष में भेजा है। इसमें यह भी है कि घर में बनाया हुआ भोजन पूरे परिवार को मिलकर करना है। विचार विमर्श के लिए एक साथ बैठना है। ऐसा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के लिए है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका, यूरोप का प्रवास करके भारत आए तो उस समय के मद्रास में उनका भाषण हुआ है। उस भाषण में पहली बार उन्होंने भारत माता पूजन का विषय रखा। उनका जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मान्यता मिली। हमने भी एक संविधान को स्वीकार किया है। इसलिए 12 जनवरी से 26 जनवरी तक इसी प्रकार का सारे देश में ऐसी छोटी-छोटी इकाई में एक परिवार, उसको हम बोलते हैं कुटुंब मित्र, वह अपने अड़ोस-पड़ोस के परिवारों के साथ इकट्ठा बैठेंगे और घर में भारत माता की प्रतिमा की पूजा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जैसे उस भाषण में कहा है कि ”पूजा करने का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। इसका भाव है कि यह सारे मनुष्य, अमीर-गरीब, किसी भी जाति या किसी भी भाषा के बोलने वाले हैं? मेरे अपने हैं। इसके साथ ही पशु, पक्षी, पौधे इन सबके प्रति प्रेम, आदर, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा रखना ही पूजा है।“ वर्ष में दो बार तो इस भाव से हम सबको मिलकर इस राष्ट्र की उन्नति के बारे में, सर्वांगीण उन्नति के बारे में सोचना है। केवल सोचना ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनकर हम अपने स्थान पर क्या योगदान दे सकते हैं? ऐसा एक वातावरण बनाना है। छोटी इकाई में हर घर के माध्यम से निर्माण करने का यह एक प्रयास, उपक्रम है। ऐसा हमने बताया है। बाकी यह जो जिला इकाई है, नगर हैं, छोटे-छोटे, यह जो कुटुंब मित्र हैं, वह अपनी-अपनी प्रेरणा से करते रहते हैं। इसके अलावा अलग-अलग त्यौहार आते हैं। यथा तुलसी विवाह आदि वर्षभर कुछ न कुछ उनका चलता रहता है। नवदंपत्ति का विषय है या विवाह योग्य आयु के युवक युवती हैं, तो आयु अनुसार ऐसे उनको छोटी इकाई में इकट्ठा करना। यानी ऐसे छोटे समूह में उनके साथ बातचीत करना, नवदंपत्ति को भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं? ऐसी 10-20 एक साथ बैठकर वैवाहिक जीवन यानी क्या है? इसकी चर्चा करना।
भारत में कश्मीर से, कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक में विवाह में सात फेरे, सप्तपदी या सात वचन यह सभी तरफ दिखाई देता है। विवाह होने के पहले उसका बोध जगाना, जानकारी देना, ऐसे छोटे-छोटे उपक्रम करना है। यदि आयु से बड़े हो गए हैं, प्रौढ़ लोग हैं, तो उनके भी साथ बैठकर अपने परिवार की भलाई के लिए सोचना मेरे स्वभाव में कुछ परिवर्तन करना है। मेरा क्या योगदान हो सकता है? छोटे बच्चों को इसी तरह कुछ कहानियां बता सकते हैं। ऐसे उपक्रम सारे देश में लगातार पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं।