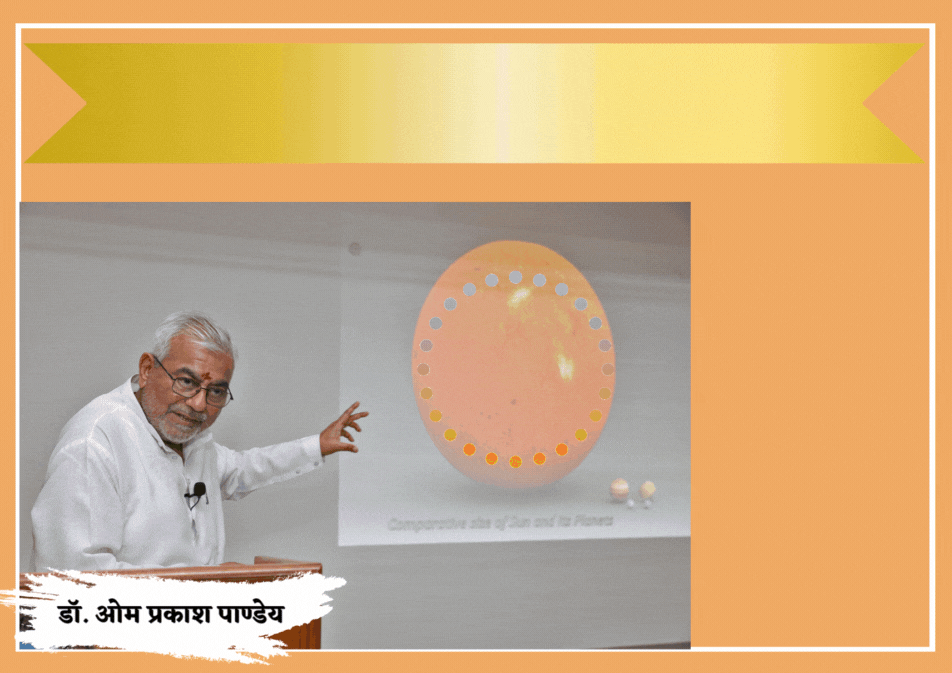वर्ष प्रतिपदा : विक्रम संवत बने राष्ट्रीय संवत
लेखक- डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय अंतरिक्ष वैज्ञानिक
हिन्दू पंचांग की प्रथम तिथि को 'प्रतिपदा' कहा जाता है। इसमें 'प्रति' का अर्थ है सामने और 'पदा' का अर्थ है पग बढ़ाना। नववर्ष का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल 'प्रतिपदा' से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्रसम्मत कालगणना व्यावहारिकता की कसौटी पर सदैव खरी उतरी है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी संकुचित विचारधारा या पंथ पर आधारित नहीं है। हम इसको पंथनिरपेक्ष रूप में देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी, देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं, ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोलशास्त्रीय सिद्धातों पर आधारित है और भारतीय कालगणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है।
वर्ष प्रतिपदा को महाराष्ट्र में 'गुड़ीपड़वा', आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 'उगादी', जम्मू-कश्मीर में 'नवरेह', पंजाब, हरियाणा में 'बैसाखी' आदि के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में 'वर्षप्रतिपदा' का विशेष महत्त्व है। भगवान ब्रह्मा जी ने इसी दिन सूर्योदय के समय सृष्टि की रचना शुरू की थी।
चक्रवर्ती सम्म्राट विक्रमादित्य की भांति भारत के दक्षिणी क्षेत्र के प्रतापी सम्राट शालिवाहन ने शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्वापित करने हेतु यही दिन चुना और विक्रम संवत के समान शक संवत की स्थापना हुई जिसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। भगवान श्री राम और महाराजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दिवस भी यही है। शक्ति और भक्ति के नवरात्र का प्रथम दिवस यही है। यह दिवस सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी की जयन्ती भी है। इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसी शुभ दिन पर संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की जयन्ती है।
आज यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में महत्वपूर्ण तिथि बनकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का पुण्य दिवस है। आज भी भारत में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के चालन संचालन में मार्च, अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय दो ऋतुओं का संधिकाल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप थर लेती है। मानव, पशु-पक्षी, यहां तक कि जड़-चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाती है। बसंतोत्सव का भी यही आधार है। प्रकृति की हरीतिमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है।
भारतीय कालगणना और पंचांग: एक अंग्रेज अधिकारी ने प. मदन मोहन मालवीय से पूछा कि "कुम्भ में इतना बड़ा जन सैलाब बगैर किसी निमंत्रण-पत्र के कैसे आ जाता है?" पंडित जी ने उत्तर दिया "छः आने के पंचांग से!"अपने देश के गाँवों, शहरों, वनों में, पहाड़ों पर या भारत के बाहर सैंकड़ों मील दूर विदेशों में हिन्दू कहीं भी रहे वह पंचांग जानता है। अपने त्यौहार, उत्सव, कुम्भ, विभिन्न देवस्थानों पर लगने वाले मेले सभी की तिथियां बगैर आमंत्रण, सूचना के उसे मालूम होती हैं। यहीं नहीं सौ वर्ष बाद किस दिन कहां कुम्भ होगा, दीपावली कब होगी, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण कब होंगे, यह भी ज्योतिषी किसी समय भी बता सकते हैं। काल की गणना दिन व रात, ऋतु तथा वर्ष के किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही की जाती रही है। वर्तमान में काल की गणना 'वर्ष' द्वारा की जाती है। परंतु प्राचीन काल में यह गणना चन्द्रमा के उदय व विकास तथा ऋतुओं के परिवर्तन द्वारा की जाती थी।
संसार के प्राचीनतम ग्रंथ 'ऋग्वेद' में एक वर्ष में तीन ऋतुओं शरद, बसंत और हेमंत का होना बताया गया है। ऋतुओं की उत्पत्ति अथवा परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। सूर्य को ऋतुओं का पिता कहा गया है। इसी कारण ऋतु चक्र, संवत्सर कहलाते हैं। एक संवत्सर में पांच ऋतुएं होती हैं और ऐसे पांच ऋतु चक्रों का एक युग होता है। इन ऋतु चक्रों के नाम हैं- संवत्सर, परिवत्सर, इडात्सर, अनुवत्सर और उद्वत्सर। इन पांच वत्सरों का गणित द्वारा अनुसन्धान कर उनका वर्णन करना पंचांग कहलाता है। सामान्य रुप से पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण बताये जाते हैं। पंचांग की मदद से आसानी से यह ज्ञात हो जाता है कि किस दिन क्या तिथि या वार है, वर्ष का आरम्भ कब हुआ, इस समय सूर्य और चन्द्रमा किस स्थान पर हैं इत्यादि इन सभी तथ्यों की जानकारी पंचांग देखने से मिलती हैं।
भारत में संवतों का प्रचलन शकों के आने के पहले वेदांग ज्योतिष के अनुसार यहां वर्ष-गणना की जाती थी लेकिन अब सूर्य सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांत के अनुसार वर्ष गणना की जाने लगी। ई. सन् 400 के लगभग तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार वर्ष गणना की जानी बिल्कुल बंद कर दी गई। ई. सन् 400 व 1200 के बीच सम्पूर्ण भारत में 'सिद्धांत ज्योतिष' के अनुसार पंचांग बनने लगे। शक संवत् का प्रचलन सर्वत्र हो गया। लेकिन 1200 के बाद जहां-जहां मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ उन्होंने लौकिक व प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्लामी हिजरी सनु का प्रचलन किया। 1757 के लगभग अंग्रेजों का भारत में राज्य स्थापन होने के समय से यहां ईसवी सन् का तिथिपत्रक, जो ग्रेगरी कैलेण्डर नाम से प्रसिद्ध है, लौकिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के साथ भारतवर्ष में इसका इतना प्रचलन हुआ कि यह एक आदत बन गया। कैलेंडर रिफार्म कमेटी स्वतंत्र भारत की सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में 'कैलेंडर रिफार्म कमेटी का गठन किया था। 1952 में "साइंस एंड कल्चर" पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार है-
ईसवी सन् का मौलिक संबध ईसाई पंथ से नहीं है। यह तो यूरोप के अर्थ सभ्य कबीलों में ईसा मसीह के बहुत पहले से ही चल रहा था।
इसके एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन होते थे।
पुरानी रोमन सभ्यता को भी तब तक ज्ञात नहीं था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या थी। यही दस महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं किया।
ईसा के 530 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, ईसाई बिशप ने पर्याप्त कल्पनाएं कर 25 दिसम्बर को ईसा मसीह का जन्म दिवस घोषित किया।
1572 में तेरहवें पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर को दस दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टूबर (शुक्रवार) को 15 अक्टूबर माना।
ब्रिटेन ने इसे दो सौ वर्ष बाद 1775 में स्वीकार किया और 11 दिन का परिवर्तन कर 3 सितम्बर को 14 सितम्बर बना दिया।
यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30 और 31 दिनों के महीने होते हैं, जो विचित्र हैं। ये न तो किसी खगोलीय गणना पर आधारित हैं और न किसी प्रकृति चक्र पर।
कैलेंडर रिफार्म कमेटी ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाने की सिफारिश की। वास्तव में विक्रम संवत, ईसा संवत से 57 साल पुराना था। परंतु तत्कालीन सरकार की 'अंग्रेजी मानसिकता' के चलते उन्हें यह सिफारिश पसंद नहीं आई।
रोमन कैलेंडर तथा इसकी विसंगतियां आज के ईसवी सन् का मूल रोमन संवत है। यह ईसा के जन्म के 753 वर्ष पूर्व रोम नगर की स्थापना से प्रारम्भ हुआ। तब इसमें 10 माह थे। (प्रथम माह मार्च से अन्तिम माह दिसम्बर तक) और वर्ष 304 दिन का होता था। बाद में रजा नूमा पिम्पोलिब्स ने दो माह (जनवरी, फरवरी) जोड़ दिए। तब से वर्ष 12 माह अर्थात् 355 दिन का हो गया। यह ग्रहों की गति से मेल नहीं खाता था, तो जुलियस सीजर ने इसे 365 दिन का करने का आदेश दे दिया। इसमें कुछ माह 30 और कुछ 31 दिन के बनाए गए और फरवरी का माह 28 दिनों का रहा जो चार वर्षों में 29 दिनों का होता है। इस प्रकार याह गणनाएं प्रारंभ से ही अवैज्ञानिक, असंगत, असंतुलित, विवादित एवं काल्पनिक रहीं।
भारतीय कालगणना प्रकृति के नियमों पर आधारित पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। इसका ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचे और वे अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दू पंचांग का उपयोग करना सीखें तो यह 'स्व' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। भारत सरकार को कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी द्वारा विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने की सिफारिश अविलंब स्वीकार करनी चाहिए।